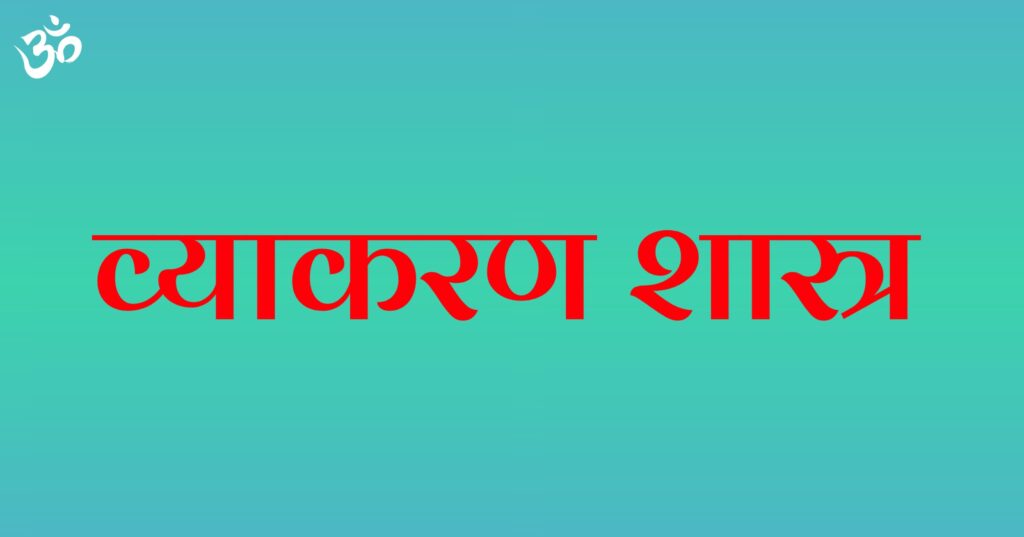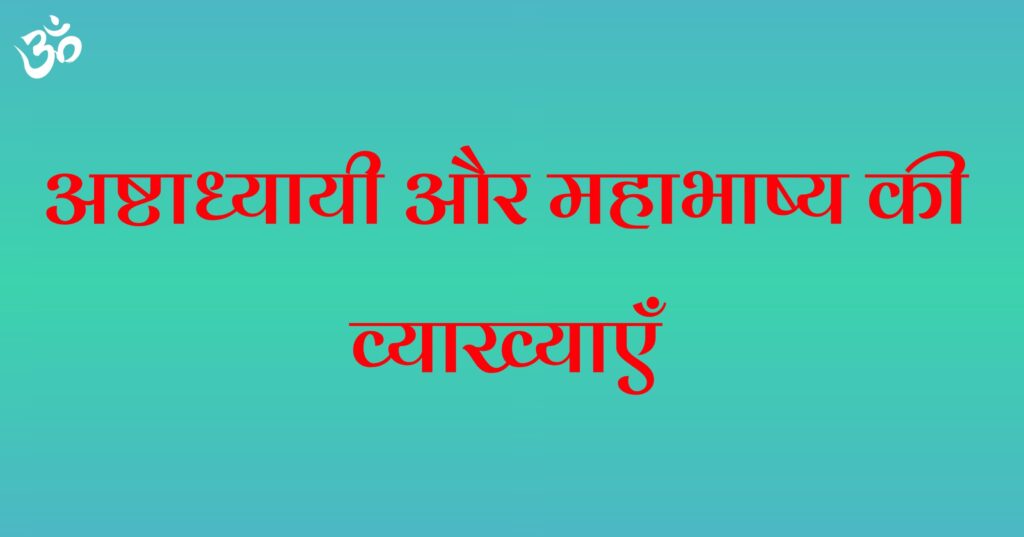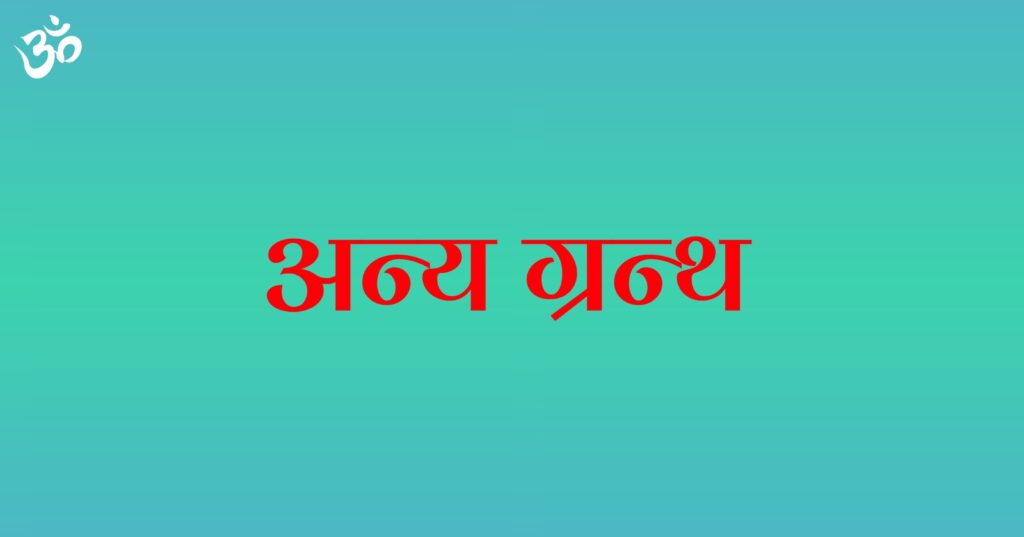Sanskrit Vyakaran ka Itihas मुखं व्याकरणं स्मृतम्। भाषा और लेखन उतना ही विशाल है और विज्ञान जितनी अनुमति देता है, उनका प्रवाह उतना ही सतत और निर्बाध है। संस्कृत भाषा दुनिया और भारत में बोली जाने वाली कई भाषाओं का एक शक्तिशाली स्रोत है। मुहावरों और समान शब्दावली के व्यापक उपयोग और विविधताओं की विविधता ने संस्कृत को एक सार्वभौमिक भाषा का दर्जा दिया है। संस्कृत शब्दावली ने संज्ञा, शीर्षक, विशेषण तथा उपसर्गों से अपनी पहचान स्थापित की है। सुबन्त और तिनन्त तथा निपात, प्रत्यय, आगम और व्याकरण के संयोजन व्यवस्थित शब्दावली को ध्वनि रूप देते हैं। व्याकरण के साथ भाषा का ऐतिहासिक और सैद्धांतिक संबंध। व्याकरण का अध्ययन भाषा अध्ययन का एक अनिवार्य हिस्सा है। व्याकरण भाषा का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह भाषा को अश्लीलता से मुक्त रखकर उसके संस्कृत स्वरूप को सुरक्षित रखता है। व्याकरण भाषा का नियामक नहीं है, यह भाषा के सहज प्रवाह को नियमों के एक समूह में बांधता है।
महर्षियों से लेकर आज के शोधकर्ताओं तक ने संस्कृत के प्रभाव और प्रतिष्ठा की प्रशंसा की है। वाक्य रचना की प्रणाली में संस्कृत ‘उद्देश्य और विविधता’ की इस बाधा से काफी हद तक मुक्त है। रामः गृहं गच्छति इन श्लोकों की स्थिति बदलने से अर्थ नहीं बदलता। संस्कृत में कर्ता, क्रिया और कृदंत – इनका अर्थ संबंधी संबंध वाक्य में शब्दों की प्रासंगिक व्यवस्था से पता चलता है। संस्कृत के इस विज्ञान ने संस्कृत को अमर बना दिया है।
व्याकरण की अनेक पुस्तकें आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखी गई हैं। जहाँ वाक्य का विश्लेषण करके वर्णों की पहचान करने की व्यवस्था है, जहाँ वर्ण से प्रारंभ करके व्युत्पत्ति दिखाकर वाक्य बनाने की व्यवस्था है। अष्टाध्यायी और प्रसेराकारम में अनेक प्रसिद्ध और विशाल व्याकरण ग्रंथ होने पर भी व्याकरण महोदधि का अमृत मंत्र अभी भी अधूरा है। संकटों और संकटों के बीच संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिए कई दार्शनिकों ने साधना की सहायता से व्याकरण ग्रंथों की रचना की है। ये सभी पुस्तकें अपने नये विश्लेषण से महान हैं।
संस्कृत व्याकरण का इतिहास (Sanskrit Vyakaran ka Itihas)
संस्कृत व्याकरण का भूमिका (Sanskrit Vyakaran ka Itihas)
Sanskrit Vyakaran ka Itihas इतिहासकारों ने भारत और संस्कृत के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। विश्व की भौगोलिक स्थिति में भारत वर्ष का अस्तित्व जितना प्राचीन है, उतना ही प्राचीन मनुष्य की ‘वाणी’ का संस्कृत रूप में प्रकट होना भी है। संस्कृत देवताओं, पितरों और मनुष्यों को जोड़ने वाली भाषा है। सम् + कृ + क्त (कर्मणि) = संस्कृतम्। (सम्भरिभ्यां करोतौ भूषणे-प. 6.1.137)। ‘कृ’ धातु से भूषण का अर्थ समझाने के लिए सम् और परि के बाद सुट् ( स् ) का प्रयोग किया जाता है।
भाषा दिव्य एवं अमर है। इसे मनुष्य तक पहुंचाने के लिए ऋषि-मुनियों ने तपस्या की है। पाणिनि आदि ऋषियों ने निरंतर ध्यान द्वारा भविष्यवाणी को सुरक्षित नियम बनाने की व्यवस्था की है। इसलिए यथार्थ में कहा गया है –
संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः (दण्डी, काव्यादर्श) ।
पाणिनि प्रभृति ने दिव्यदर्शन की शक्ति से शब्दों के स्वरूप, विभिन्न आदि-विभागों का निर्धारण किया और शिष्य परंपरा के माध्यम से विज्ञान सम्मत प्रवृत्ति को आज तक जीवित रखा है। पाणिनि ने सूत्रों के माध्यम से भाषा का निर्माण किए बिना वर्तमान भाषा के सीमित स्वरूप को संरक्षित करने की एक व्यवस्थित विधि का आविष्कार किया है। इसीलिए संस्कृत सुरक्षित रही और इसने कई अन्य भाषाओं की शब्दावली को प्रभावित किया है। कई भारतीय भाषाओं और भारतीयों की भाषाओं के साथ संस्कृत की भाषाई निकटता ने संस्कृत को वैश्वीकरण की प्राथमिक ध्वनि के रूप में स्थापित किया है।
व्याकरणशास्त्र (Sanskrit Vyakaran ka Itihas)
Sanskrit Vyakaran ka Itihas पदों का विश्लेषण (व्युत्पत्ति) तथा शुद्धता की समीक्षा के अर्थ में व्याकरण का उद्भव वैदिक युग में ही हो चुका था। इसके अनुसन्धान की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।’ वेदाध्ययन के लिए उपादेय शास्त्रों (वेदाङ्गों) में व्याकरण को प्रमुख स्थान मिला (मुखं व्याकरणं स्मृतम्)। पद- विवेचन में अन्य सभी भाषाओं में संस्कृत अग्रणी है, इतनी सूक्ष्म दृष्टि तथा गम्भीरता से व्याकरण का विचार कहीं नहीं है। वेदाङ्गों में शिक्षा का उपयोग शुद्ध शब्दोच्चारण के लिए, व्याकरण का पद के विवेचन के लिए और निरुक्त का अर्थज्ञान एवं निर्वचन के लिए था। कालक्रम से ये सभी उपयोग व्याकरण पर आश्रित हो गये, उसका भार बढ़ गया। व्याकरण की दो पद्धतियाँ वैदिक युग में थीं और दोनों से शुद्ध पदों के ज्ञान का लक्ष्य पूरा होता था- (क) प्रतिपद-पाठ तथा (ख) सामान्य-विशेष नियमों से शब्द-ज्ञान देना। प्रातिशाख्यों में दोनों प्रकार की विधियाँ मिलती हैं। क्रमश: दूसरी विधि की उपादेयता अधिक स्पष्ट हुई तो प्रतिपद-पाठ की निन्दा होने लगी क्योंकि उसमें काल का अपव्यय माना गया।
यद्यपि अनेक वैयाकरणों के नाम तथा उनके सिद्धान्त ७०० ई० पू० के आसपास रचे गये निरुक्त में मिलते हैं, तथापि उनके ग्रन्थों की प्राप्ति नहीं हुई है। तैत्तिरीय संहिता (६/४/७/३) के अनुसार देवों की प्रार्थना मानकर इन्द्र ने अव्याकृत वाणी का विश्लेषण करके प्रथम वैयाकरण होने का श्रेय प्राप्त किया। वाक्य से पदों का अपोद्धार और पद में प्रकृति एवं प्रत्यय की कल्पना व्याकृत वाणी का लक्षण हुई। इसे व्याकरण का शब्दपक्ष अर्थात् व्यावहारिक पक्ष कहा गया। दूसरी ओर व्याकरण का अर्थपक्ष अर्थात् दार्शनिक पक्ष भी था जिसमें वाक्य और उसका अर्थ ही परमतत्त्व माना गया। फिर भी व्याकरण की प्रक्रिया तो मुख्य रूप से शब्दपक्ष वाली ही है जिसमें परमतत्त्व वाक्य का विभाजन पदों से होते हुए छोटी-छोटी इकाइयों में किया जाता है, एक-एक वर्ण की व्यवस्था की जाती है। यही संस्कृत भाषा की विशिष्टता है कि वैयाकरणों ने किसी वर्ण को अव्याख्यात नहीं छोड़ा।
आरम्भिक वैयाकरण निश्चित रूप से वैदिक भाषा का अन्वाख्यान करते थे, क्रमशः लौकिक (संस्कृत) और वैदिक दोनों भाषाओं के अन्वाख्यान में वे सन्नद्ध हुए और अन्ततः उनका लक्ष्य केवल संस्कृत भाषा की व्याख्या में ही परिमित हो गया। पाणिनि-जैसे आठ आदिम वैयाकरण हुए जिन्होंने पृथक् पृथक् व्याकरण-सम्प्रदायों का प्रवर्तन किया। बोपदेव (१३ वीं शताब्दी ई०) ने अपने ‘कविकल्पद्रुम’ नामक ग्रन्थ के आरम्भ में इनके नाम दिये हैं जो वस्तुत: पक्षपातपूर्ण हैं-
इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः ।
पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टादि-शाब्दिकाः ॥
इन सभी व्याकरण-प्रस्थानों में पाणिनीय प्रस्थान गम्भीरता, व्यापकता तथा ग्रन्थ-बाहुल्य की दृष्टि से प्रशस्त है। यहाँ मुख्य रूप से पाणिनीय प्रस्थान के महत्त्वपूर्ण आचार्यों तथा उनकी कृतियों का परिचय दिया जाता है।
(१) पाणिनि (Sanskrit Vyakaran ka Itihas)
Sanskrit Vyakaran ka Itihas संस्कृत भाषा को अद्भुत व्याकरण का उपहार देनेवाले पाणिनि का जन्म शालातुर-ग्राम (वर्तमान – लाहुर, पाकिस्तान में अटक के समीप) में हुआ था, इसीलिए पतञ्जलि ने इन्हें प्रायः ‘शालातुरीय’ कहा है। इनकी माता का नाम दाक्षी था, अतः ये ‘दाक्षीपुत्र’ भी कहे गये हैं। कथासरित्सागर के अनुसार ये वर्ष नामक आचार्य के शिष्य थे। पाणिनि-काल ५०० ई० पू० में अधिसंख्यक विद्वानों ने माना है किन्तु कुछ लोग इन्हें ७००-६०० ई० पू० के बीच रखने के पक्षधर हैं। डॉ० बेलवलकर इसी मत के प्रवर्तक थे। पाणिनि ने सम्भवतः ‘जाम्बवतीजय’ काव्य भी लिखा था।
पाणिनि का काल (Sanskrit Vyakaran ka Itihas)
Sanskrit Vyakaran ka Itihas यह बहुत जटिल प्रश्न है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इसका समाधान अपने-अपने तर्को से किया है।
(१) पाणिनि के काल की पूर्वसीमा यास्क का निरुक्त (८०० ई० पू०) तथा प्रातिशाख्य- ग्रन्थ हैं जो पाणिनि से पूर्व की रचनाएँ हैं। उनके समय की उत्तर सीमा नन्दकाल में आविर्भूत कात्यायन (३५० ई०पू०) हैं जिन्होंने पाणिनीय सूत्रों पर वार्तिक लिखे हैं।
(२) बृहत्कथा की परम्परा में पाणिनि और कात्यायन को समकालिक कहा गया है जिसे प्रमाण मानकर मैक्समूलर आदि पाश्चात्त्य लेखकों ने पाणिनि को भी ३५० ई० पू० में रखा था। किन्तु यह दोषपूर्ण मान्यता है क्योंकि कात्यायन के वार्तिकों से स्पष्ट होता है कि पाणिनि के द्वारा निरीक्षित संस्कृत भाषा में उल्लेखनीय परिवर्तन कात्यायन के समय तक हो चुके थे, अत: दोनों के काल में दो-तीन सौ वर्षों का व्यवधान अवश्य होगा अर्थात् पाणिनि को ६०० ई० पू० मानना अनिवार्य है।
(३) कुछ लोगों ने ‘कुमारः श्रमणादिभिः’ (पा० सू० २/१/७०) के आधार पर पाणिनि पर बौद्ध प्रभाव दिखाया है क्योंकि उक्त सूत्र के गण-पाठ में स्त्रीलिङ्ग ‘श्रमणा’ शब्द आया है। बुद्ध ने ही श्रमण का प्रयोग करके स्त्रियों को भी श्रमणा (संन्यासिनी) बनने का विधान किया था। यह तर्कसंगत नहीं क्योंकि प्राचीन ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी’ श्रमण’ का प्रयोग है।
(४) पाणिनि ने ‘निर्वाणोऽवाते’ (पा० सू० ८/ २/५०) सूत्र में ‘निर्वाण’ शब्द (त का नकार) का विधान ‘शान्त या बुझा हुआ’ के अर्थ में किया है- निर्वाणोऽग्रिः, निर्वाणः प्रदीपः। बौद्ध धर्म में यह मोक्ष के अर्थ में अत्यन्त प्रसिद्ध शब्द है जो तृतीय आर्यसत्य माना गया है। बौद्ध धर्म से पाणिनि परिचित होते तो इस शब्द को इस अर्थ में अवश्य समझाते।
(५) गोल्डस्टूकर तथा रामकृष्ण भण्डारकर ने पाणिनि का काल ७०० ई० पू०, श्रीपादकृष्ण बेलवलकर ने ७००-६०० ई० पू० तथा वासुदेव शरण अग्रवाल ने ५०० ई० पू० के निकट माना है। डॉ० अग्रवाल ने तो पाणिनि की आयु ७० वर्ष मानकर उनके जीवन-काल को निश्चित तिथियों के द्वारा निरूपित किया है। यहाँ न तो मैक्समूलर, कीथ आदि के द्वारा स्वीकृत ३५० ई. पू. को और न ही युधिष्ठिर मीमांसक के द्वारा निर्दिष्ट २९०० ई. पू. को पाणिनि का काल माना जा सकता है – ये अतिवादी मत हैं।
गोल्डस्टूकर ने पाणिनि के वैदिक ज्ञान की मीमांसा करते हुए कहा था कि वे केवल तीन वेदों से परिचित थे; आरण्यक, उपनिषद्, प्रातिशाख्य, शतपथ, अथर्ववेद आदि से वे अपरिचित थे। इस मत का विस्तृत निराकरण पॉल थीमे, अग्रवाल आदि ने किया है। वे मानते हैं कि सम्पूर्ण वेद-वाङ् मय पाणिनि के पूर्व विकसित हो चुका था। यह काल अवश्य ही ६०० ई. पू. का रहा होगा। उस काल में संस्कृत में प्राच्य और उदीच्य नामक दो विभाषाएँ (बोलियाँ) प्रचलित थीं।
पाणिनि का योगदान (Sanskrit Vyakaran ka Itihas)
Sanskrit Vyakaran ka Itihas संस्कृत व्याकरणशास्त्र को पाणिनि का योगदान अमर है। इनका व्याकरण-प्रस्थान संस्कृत व्याकरण के सभी दस उपलब्ध प्रस्थानों में व्यापकता, गम्भीरता एवं स्वीकार्यता के कारण अग्रणी है। लौकिक संस्कृत के साथ वैदिक भाषा की तुलना एवं उनके शब्दों की सूक्ष्म विवेचना इनके व्याकरण की विशिष्टता है। अपनी प्रख्यात कृति ‘अष्टाध्यायी’ में इन्होंने ३९७८ सूत्रों (तथा १४ प्रत्याहार-सूत्रों) के द्वारा तात्कालिक भाषा का जैसा सर्वेक्षण इन्होंने किया है, वैसा किसी भाषा के किसी ग्रन्थ में नहीं है। अष्टाध्यायी आठ अध्यायों में विभाजित सूत्र-ग्रन्थ है, प्रत्येक अध्याय को ४-४ पादों में विभक्त किया गया है। विषयों का क्रम प्रकरणों के अनुसार, अनुवृत्ति को ध्यान में रखकर, वैज्ञानिक ढंग से रखा गया है। यह अपरिचित भाषा को सिखाने वाली रचना नहीं है, अपितु परिचित-प्रचलित भाषा के पदों का विवरण देने वाली कृति है। लोक तथा वेद में व्यवहृत प्रत्येक पद के प्रत्येक अक्षर की व्याख्या करना इसका लक्ष्य है।
अष्टाध्यायी को समझने के लिए उन्होंने कुछ सहायक ग्रन्थ भी परिशिष्ट के रूप में लिखे- गणपाठ, धातुपाठ, लिङ्गानुशासन तथा उणादिसूत्र। इन पाँचों का संयुक्त नाम है- पञ्चपाठी। इस प्रकार पाणिनि ने अपने व्याकरण-प्रस्थान का प्रवर्तन इसे सर्वाङ्गपूर्ण बनाने के महान् उद्देश्य से किया था। यह कहा जाता है कि संस्कृत की समस्त शब्द-सम्पदा नष्ट हो जाये तो भी अष्टाध्यायी के द्वारा उसका पुनरुद्धार हो जा सकता है। पाणिनि के भाषिक तथा व्याकरणिक योगदान का आकलन निम्नांकित बिन्दुओं पर किया जा सकता है:-
(१) – माहेश्वर-सूत्र या प्रत्याहार-सूत्र अष्टाध्यायी के आधार हैं। ये वर्णोपदेश के रूप में हैं जिनसे वर्ण-संक्षेप के लिए प्रत्याहार बनते हैं जैसे अणू, अच्, हल्, अक्, जश् आदि। उक्त १४ सूत्रों में संस्कृत की वर्णमाला अष्टाध्यायी के सूत्रों में उपयोग के लिए दी गयी है। स्वरों को मूल (अ,इ,उ,ऋ.लू) तथा सन्ध्यक्षर (ए ओ ए औ) के रूप में बाँटकर व्यञ्जनों को अन्तःस्थ, स्पर्श (विपरीत क्रम से पंचम, चतुर्थ तृतीय, द्वितीय और प्रथम के रूप में) तथा ऊष्म के क्रम से सजाकर ध्वनिविज्ञान के क्षेत्र में समर्थ पद स्थापित किया गया है।
(२) – अष्टाध्यायी में लाघव के लिए अनेक विधियों का प्रयोग है जैसे – प्रत्याहार, गण-व्यवस्था, अनुबन्धों का विभिन्न प्रयोजनों से विनियोग, अधिकार-सूत्र, अनुवृत्ति तथा परिभाषा-सूत्र।’ प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों तक ही परिमित नहीं (जैसे- अच् – सभी स्वरवर्ण, जश् – तृतीय वर्ण, शल् ऊष्मवर्ण इत्यादि), प्रत्युत सुप्, तिङ्, सुट् इत्यादि के रूप में प्रत्यय-समूह भी इसकी परिधि में आते हैं। दो वर्णों का प्रत्याहार अनेक वर्णों का लाघव करता है।
(३) – सन्धि के नियमों को अष्टाध्यायी के षष्ठ और अष्टम अध्यायों में पाणिनि ने विस्तार से समझाया है। इस प्रसंग में षत्व, णत्व, जश्त्व, चर्व आदि सभी प्रकार के वर्ण-परिवर्तन स्पष्ट किये गये हैं।
(४) – व्याकरण की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया उत्सर्ग (सामान्य नियम) तथा अपवाद (विशेष नियम) के रूप में पाणिनि ने अपनायी है जैसे- दीर्घ होने का सामान्य नियम देकर पुनः अपवाद के कई सूत्र दिये गये हैं कि इन स्थानों में दीर्घ का प्रसंग होने पर भी वह नहीं होगा। इससे व्याकरण में प्रतिपद-पाठ की प्रलम्ब विपत्ति का निराकरण हो जाता है।
(५) – पद-विज्ञान ही पाणिनि का मुख्य प्रतिपाद्य है। पद दो प्रकार के हैं- सुबन्त तथा तिङन्त। प्रातिपदिकों से सुबन्त और धातुओं से तिङन्त पद निष्पन्न होते हैं। कुछ प्रातिपदिक कृदन्त, तद्धितान्त और समास के रूप में हैं। इन सभी की निष्पत्ति की सूक्ष्म प्रक्रिया अष्टाध्यायी में वर्णित है। पद का रूप चाहे सरल हो या जटिल, पाणिनि उसका प्रत्यक्षर विवरण देते हैं। आधुनिक वर्णनात्मक भाषाशास्त्र का प्रवर्तक पाणिनि को माना जाये तो अत्युक्ति नहीं होगी। अव्याकृत पदों (अव्ययों-निपातों) को पाणिनि ने प्रतिपद-पाठ का ही परिधान प्रदान किया है।
(६) – प्रत्ययों का विधान या वर्णन करते हुए पाणिनि का ध्यान अर्थ पर भी रहा है। ऐसा मुख्यतः कृत् और तद्धित के प्रसंग में देखा जा सकता है। प्रत्ययान्त धातु के निष्पादक सन्, क्यच्, यङ् आदि प्रत्ययों के भी विशिष्ट अर्थ उन्होंने बताये हैं। धातुपाठ पूरा का पूरा अर्थ से विभूषित है। इस प्रकार अर्थविज्ञान के क्षेत्र में भी पाणिनि का योगदान अमूल्य है।
(७) – पाणिनि ने पारिभाषिक शब्दों का द्विविध प्रयोग किया है। कुछ शब्द तो सामान्य व्यवहार से लेकर विशिष्ट अर्थों में उन्होंने रखे हैं जैसे- गुण, वृद्धि, धातु, प्रातिपदिक आदि। कुछ सर्वथा कृत्रिम लघुकाय संज्ञाएँ रखीं जैसे- टि, घु, भ, घ इत्यादि। इनकी भाषा के लाघव में प्रभूत भूमिका है। (८) पाणिनि भाषा का विश्लेषण एक समृद्ध दार्शनिक आधार पर कर रहे थे। कात्यायन, पतञ्जलि, भर्तृहरि आदि परवर्ती व्याख्याकारों ने पाणिनि के दार्शनिक सिद्धान्तों को समझाते हुए स्पष्ट कहा है कि व्याकरण भाषा का केवल बाह्य विश्लेषण नहीं है, इसमें वाक्-रूपी ब्रह्म की अभिव्यक्ति भी होती है।
अन्य व्याकरण-सम्प्रदाय जहाँ भाषा की ऊपरी रूपरेखा तक ही सीमित हैं, पाणिनीय तन्त्र अर्थपक्ष (अर्थात् दर्शन) का भी विवेचन करता है। इस प्रकार एक महत्त्वपूर्ण प्रस्थान के प्रवर्तक पाणिनि का अद्भुत योगदान है।
(२) कात्यायन (Sanskrit Vyakaran ka Itihas)
Sanskrit Vyakaran ka Itihas पाणिनीय सूत्रों की समीक्षा लघुकाय वार्तिकों में करनेवाले कात्यायन का काल ३५० ई. पू. माना जाता है। इनका एक नाम वररुचि भी था (यद्यपि इस नामके अनेक लेखक हुए हैं)। ये दाक्षिणात्य थे जैसा कि पतञ्जलि ने इनके एक वार्तिक (यथा लौकिकवैदिकेषु) की समीक्षा में कहा है- प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः। पाणिनि के व्याकरण में काल-गत व्यवधान से कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हो गयी थी जिसे वार्तिकों में (उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्ता वार्तिकम्-काव्यमीमांसा) निरूपित किया गया है। जैसे- पाणिनि के समय दीधी और वेवी धातुएँ प्रयुक्त थीं, कात्यायन के काल में अप्रचलित हो गयीं। ‘इन्धिभवतिभ्यां च’ इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है; इसी प्रकार भाषा के विकास का निरीक्षण वार्तिकों में है। संस्कृत की विभाषाओं का निर्देश, लोकव्यवहार को भाषा का नियामक बताना एवं शब्दार्थ का नित्य सम्बन्ध मानना (सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे) कात्यायन का विशिष्ट योगदान है। महाभाष्य में समस्त वार्तिकों की समीक्षा है, उसी से वार्तिकों का स्वरूप और परिमाण जाना जाता है।
(३) पतञ्जलि (Sanskrit Vyakaran ka Itihas)
Sanskrit Vyakaran ka Itihas व्याकरण महाभाष्य के लेखक पतञ्जलि ने अपने लिए ‘गोनर्दीय’ और ‘गोणिकापुत्र’ का प्रयोग किया है। इससे ज्ञात होता है कि ये गोनर्द (गोंडा-उत्तरप्रदेश) के निवासी थे तथा इनकी माता का नाम गोणिका था। कुछ विद्वानों ने इन्हें कश्मीरी कहा है। प्राय: माना जाता है कि इन्होंने ही ‘योगसूत्र’ की रचना की थी। कुछ प्राचीन विद्वान् तो इन्हें आयुर्वेद के ग्रन्थ ‘चरकसंहिता ‘का भी लेखक या संस्कर्ता मानते हैं। इस सन्दर्भ में एक प्राचीन पद्य है-
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन।
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ।।
केवल योगसूत्र और महाभाष्य की एककर्तृकता प्रमाणों से पुष्ट होती है।
पतञ्जलि का समय अधिक विवादास्पद नहीं। प्रायः सभी विद्वान् इन्हें २०० ई. पू. से १५० ई. पू. तक मानने में सहमत हैं। केवल पं. युधिष्ठिर मीमांसक इन्हें २००० ई. पू. मानने के पक्षधर हैं किन्तु यह अतिवादी मत है।’ पतञ्जलि के काल-निर्णय का सबसे पुष्ट प्रमाण पुष्यमित्र (शुंगनरेश) के द्वारा संचालित अश्वमेध यज्ञ है जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है और पतञ्जलि भी निर्दिष्ट करते हैं- पुष्यमित्रो यजते, याजका याजयन्ति। तत्र भवितव्यम्-पुष्यमित्रो याजयति, याजका याजयन्तीति । स्पष्टतः पुष्यमित्र के अनेक पुरोहितों में पतञ्जलि भी थे। उसी काल में महाभाष्य की रचना हुई थी। इतिहासकार मानते हैं कि अन्तिम मौर्य-नरेश को मारकर उनके सेनापति पुष्यमित्र ने १८५ ई. पू. में मगध का राज्य आत्मसात् किया था। मत्स्यपुराण के निर्देश से पता लगता है कि ३६ वर्षों तक राज्य करने के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। यह समय १४९ या १५० ई. पू. होता है। अतः यही काल महाभाष्य की रचना का है। उस समय कुछ ही दिन पूर्व किसी यवन आक्रान्ता ने साकेत तथा माध्यमिका नगरों पर घेरा डाला था। इसका उल्लेख पतञ्जलि करते हैं- अरुणद् यवनो माध्यमिकाम्; अरुणद् यवनः साकेतम्।
पतञ्जलि का योगदान (महाभाष्य का महत्त्व) (Sanskrit Vyakaran ka Itihas)
Sanskrit Vyakaran ka Itihas पतञ्जलि ने पाणिनि के महत्त्वपूर्ण सूत्रों तथा उनपर कात्यायन के वार्तिकों की समीक्षा महाभाष्य में की है। समीक्षा के क्रम में उन्होंने इतिहास, धर्म, समाज, राजनीति, लोकप्रथा इत्यादि अनेक विषयों पर प्रकाश डाला है। जैसे- अपने युग की घटनाओं (यवनों का साकेत पर घेरा डालना), अभिनयों (कंसं घातयति, बलिं बन्धयति) तथा साहित्यिक रचनाओं (वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, भैमरथी नामक आख्यायिकाओं) का उल्लेख। इस प्रकार महाभाष्य में पतञ्जलि ने तात्कालिक सांस्कृतिक परिवेश में झाँकने के लिए पर्याप्त सामग्री दी है।
भाष्य का लक्षण है-
सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः।
स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥
सूत्रों का अनुसरण करने वाले पदों से सूत्रार्थ का विवरण (व्याख्या) देते हुए जब कोई अपने पदों का भी व्याख्यान करता है तब इसे ‘भाष्य’ कहते हैं। यद्यपि संस्कृत शास्त्रों में कई भाष्य हैं जैसे- शाबरभाष्य, शांकरभाष्य, रामानुजभाष्य, सायणभाष्य आदि, किन्तु महाभाष्य कहलाने का गौरव पातञ्जल भाष्य को ही मिला है। यह इसकी महत्ता का सूचक है। उपर्युक्त विषय-वैविध्य इसका निमित्त है। ‘वाक्यपदीय’ में (२/४७७) भर्तृहरि ने पतञ्जलि की प्रशंसा में कहा है-
कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना ।
सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥
यहाँ पतञ्जलि को ‘तीर्थदर्शी’ (व्याकरण के अतिरिक्त अन्य आगमों का ज्ञाता) कहा गया है; महाभाष्य सभी लौकिक युक्तियों तथा परिभाषाओं के संकेतों (न्याय + बीज) से सम्पन्न है। इस सन्दर्भ में व्याख्याकार पुण्यराज ने कहा है- तच्च भाष्यं न केवलं व्याकरणस्य निबन्धनं यावत्सर्वेषां न्यायबीजानां बोद्धव्यमिति अत एव सर्वन्यायबीजहेतुत्वादेव महच्छब्देन विशेष्य महाभाष्यमित्युच्यते लोके (वाक्य, टीका २/४७७)। इसमें अनेक प्रकार के सिद्धान्त हैं, विद्यावाद हैं और दर्शनों की लोकोक्तियाँ हैं (महाभाष्यं हि बहुविधविद्यावादबलमार्षं व्यवस्थितम्-वा०प० टीका २/४७८)। जैसे- व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्नहि सन्देहादलक्षणम्।’ यह सिद्धान्त व्याकरण के अतिरिक्त भी कई शास्त्रों में उपादेय है। इसी प्रकार कई न्याय उन्होंने दिये हैं जैसे- एकदेशविकृतमनन्यवत्, पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः इत्यादि।
महाभाष्य के प्रथम आह्निक के द्वारा पतञ्जलि ने भूमिका-लेखन की यास्कीय विधि को विकसित किया। यास्क निरुक्त के प्रथमाध्याय के रूप में शास्त्र की पूर्वपीठिका (भूमिका) की परम्परा का प्रवर्तन कर चुके थे। महाभाष्य के प्रथम आह्निक को ‘पस्पशा’ (विमर्श) कहते हैं; इसमें शब्द और अर्थ का स्वरूप, व्याकरण के प्रयोजन, शब्दानुशासन की प्रक्रिया, शब्दार्थ-सम्बन्ध, व्याकरण का स्वरूप तथा अइउण् आदि सूत्रों में वर्णोपदेश का महत्त्व- इस प्रकार आवश्यक विषयों का गम्भीर विवेचन सरल शैली में किया गया है। महाभाष्य में व्याकरण का शब्द-पक्ष और अर्थपक्ष (दर्शन)- दोनों विवेचित हैं, भर्तृहरि ने दार्शनिक पक्ष को आधार बनाकर ‘वाक्यपदीय’ की रचना की। पतञ्जलि के समक्ष अनेक सिद्धान्त थे; किसी एक मत को स्वीकार न करके उन्होंने यत्र-तत्र अपनी उदारता भी प्रकट की। उनका कथन है- सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्, तत्र नैकः पन्था शक्य आस्थातुम्। इसीलिए उन्होंने पस्पशाह्निक में आकृति और द्रव्य दोनों को पदार्थ मानकर सूत्र-प्रवृत्ति दिखायी है। व्याकरण के स्वरूप के सम्बन्ध में उनके समक्ष तीन पक्ष थे- सूत्रं व्याकरणम्, शब्दो व्याकरणम्, लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्। अन्तिम पक्ष उन्हें मान्य हुआ, अन्य दोनों के दोष उन्होंने दिखाये।
पतञ्जलि का एक सर्ववेदपारिषद वाक्य व्याख्यान का स्वरूप स्पष्ट करता है- न केवलानि चर्चापदानि व्याख्यानम्, किं तहिं? उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहारः- इत्येतत्समुदितं व्याख्यानं भवति (आह्निक-१ )। इसका पालन करते हुए उन्होंने पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष की भी विवेचना की है। सूत्र की विविध-कोटिक समीक्षा महाभाष्य का वैशिष्ट्य है।
भाष्यकार को लोक-प्रचलित भाषा और उनकी विभाषाओं का भी ध्यान है। आधुनिक भाषाशास्त्री के समान पतञ्जलि भी लोक में प्रयुक्त भाषा को साहित्यिक भाषा से अधिक महत्त्व देते हैं। भाषा में स्थानीय अर्थभेद और प्रयोगभेद होते हैं- इसकी विवेचना उन्होंने अनेकत्र की है। ध्वनि, पद और अर्थ के रूप में भाषा के समस्त गूढ सिद्धान्तों का अनुशीलन महाभाष्य में सुलभ है। वस्तुतः पतञ्जलि अपने युग से आगे देखने वाले महामनीषी थे, पाणिनीय तन्त्र उनसे प्रतिष्ठित हुआ।
व्याकरणशास्त्र में पाण्णिनि, कात्यायन तथा पतञ्जलि को ‘त्रिमुनि’ कहा जाता है। इस पाणिनीय तन्त्र को ‘त्रिमुनि व्याकरणम्’ के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। इन मुनियों में भी सिद्धान्त की दृष्टि से क्रमशः प्रामाणिकता बढ़ती गयी है- यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्। इस दृष्टि से पतञ्जलि का महत्त्व उपर्युक्त दोनों आचार्यों से बढ़कर है।
जीवित भाषा की दृष्टि से इन तीन वैयाकरणों में ही व्याकरण की समाप्ति हो गयी क्योंकि भाषा के तथ्यों का निरीक्षण आगे नहीं हुआ। पाणिनि तथा पतञ्जलि की व्याख्या एवं सूत्र-क्रम- भञ्जक प्रक्रिया-ग्रन्थों की श्रृंखला ही परवर्ती पाणिनीय सम्प्रदाय की विशिष्टता है।
(४) भर्तृहरि तथा वाक्यपदीय (Sanskrit Vyakaran ka Itihas)
Sanskrit Vyakaran ka Itihas पाणिनीय व्याकरण-तन्त्र में वैयाकरण-दार्शनिक भर्तृहरि का अनुपम स्थान है। इन्होंने ‘वाक्यपदीय’ के रूप में व्याकरण-दर्शन की एक अद्भुत कृति के द्वारा अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। महाभाष्य में निरूपित दार्शनिक सिद्धान्तों तथा अर्थविज्ञान के नियमों का पद्यात्मक (कारिकाओं के रूप में) विवेचन वाक्यपदीय में है। इसके अतिरिक्त महाभाष्य की व्याख्या भी (दीपिका-नामक) भर्तृहरि ने लिखी थी जिसके प्रथम सात आह्निक प्रकाशित हैं।’ सम्भवत: उन्होंने केवल तीन पादों की व्याख्या लिखी थी।
भर्तृहरि के काल पर इधर पर्याप्त विचार हुए हैं। पहले लोग इनका काल इत्सिंग के निर्देश के अनुसार ६५० ई. के कुछ पूर्व मानते थे। किन्तु देश-विदेश के अनेक विद्वानों ने पुष्ट प्रमाणों के आधार ४५०-५००ई. के बीच इनका काल अब स्वीकार कर लिया है। स्कन्दस्वामी के निरुक्तभाष्य में वाक्यपदीय का उद्धरण, पुण्यराज की वाक्यपदीय टीका (२/४८६ तथा ४८९) में भर्तृहरि के गुरु का नाम वसुरात का उल्लेख, बौद्ध दार्शनिक दिङ्नाग की त्रैकाल्यपरीक्षा (सम्प्रति तिब्बती के उपलब्ध) में वाक्यपदीय के प्रथम श्लोक की स्वोपज्ञवृत्ति का निर्देश, जैन न्याय के विद्वान् मल्लवादिन् के ‘द्वादशार-नय-चक्र’ में भर्तृहरि का उल्लेख ये ऐसे प्रमाण हैं जो इन्हें ४५०- ५०० ई. के बीच स्वीकार करने को विवश करते हैं।
वाक्यपदीय तीन काण्डों में विभक्त है- ब्रह्मकाण्ड (१५६ कारिकाएँ), वाक्यकाण्ड (४८६ कारिकाएँ) तथा प्रकीर्णकाण्ड या पदकाण्ड (१४ समुद्देशों में विभक्त, १३२३ कारिकाएँ)।’ प्रथम काण्ड पर हरिवृषभ, द्वितीय काण्ड पर पुण्यराज एवं तृतीय काण्ड पर हेलाराज की व्याख्याएँ मिलती हैं। ब्रह्मकाण्ड पर भर्तृहरि ने स्वोपज्ञवृत्ति भी लिखी थी। वाराणसी के विद्वान् पं. रघुनाथ शर्मा ने सम्पूर्ण वाक्यपदीय की अभिनव’ अम्बाकर्ती’ व्याख्या लिखी है। ब्रह्मकाण्ड शब्दब्रह्म तथा स्फोट का विवेचन करता है, इसमें वाणी के तीन स्तरों (पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी) का निर्देश है। अपभ्रंश शब्दों से अर्थबोध का कारण साधुशब्दों का स्मरण है। व्याकरण शब्द के साधुत्व का नियामक है। वाक्यकाण्ड में वाक्य-स्वरूप पर विस्तृत विवेचना करते हुए इसके विविध लक्षणों का विमर्श किया गया है। वाक्य-स्वरूप के आठ पक्ष हैं- आख्यात शब्द, पदसंघात, संघातवर्तिनी जाति, अनवयव एकशब्द, क्रम, बुद्धि से कल्पना करके पदों का अनुसंहार, आद्य पद तथा सर्वसाकांक्ष पद वाक्य हैं (वा. प. २/१-२) । तृतीयकाण्ड विविध विषयों का विवेचन-परक होने से ‘प्रकीर्णकाण्ड’ कहलाता है। इसे पदकाण्ड भी कहते हैं क्योंकि सभी विषय ‘पद’ के चारों ओर भ्रमण करते हैं। ये विषय ‘समुद्देश’ रूप है जैसे- जातिसमुद्देश, द्रव्यसमुद्देश, सम्बन्धसमु., भूयोद्रव्यसमु., गुणसमु. दिक्समु. साधनसमु. (कारक), क्रिया., काल., पुरुष, संख्या. (वचन), उपग्रह. (आत्मनेपद-परस्मैपद), लिङ्ग तथा वृत्तिसमुद्देश। अन्तिम समुद्देश सबसे बड़ा है (६२७ कारिकाएँ)। वाक्यपदीय के ब्रह्मकाण्ड को शब्द-दर्शन की पूर्वपीठिका मानकर शेष दो काण्डों में क्रमशः वाक्य एवं पद का दार्शनिक विचार होने से इस ग्रन्थ का शीर्षक अन्वर्थ है। भर्तृहरि का व्याकरण-दर्शन में अमूल्य योगदान है।
(५) अष्टाध्यायी और महाभाष्य की व्याख्याएँ (Sanskrit Vyakaran ka Itihas)
Sanskrit Vyakaran ka Itihas पाणिनीय अष्टाध्यायी पर अनेक वृत्तियों या टीकाग्रन्थों के रचे जाने की सूचना प्राप्त होती है किन्तु उन सबमें उपलब्ध प्रथम वृत्ति ‘काशिका’ ही है जिसे जयादित्य (१-५ अध्यायों पर) तथा वामन (६-८ अध्यायों पर) ने लिखा था। काशिकावृत्ति (१/३/२३) में भारविकृत किरातार्जुनीय के एक पद्य (३/१४) का खण्ड उद्धृत है- संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यः। इस आधार पर भारवि (५५०-६०० ई.) के समय या उनके बाद इस वृत्ति का काल होगा। काशिका पर प्रथम टीका जिनेन्द्रबुद्धि ने लिखी थी जिनका काल ७०० ई. माना जाता है, अत: काशिका का रचनाकाल ६००-६५० ई. के बीच सामान्यत: माना जाता है। इस वृत्ति में पाणिनीय सूत्रों की विस्तृत व्याख्या अनुवृत्ति-निवृत्ति को दिखाते हुए की गयी है, गण-पाठ को भी पूर्णतः व्याख्या में समाविष्ट किया गया है। वार्तिकों को भी यथास्थान रखकर काशिका में समझाया गया है। इसके मङ्गलाचरण में ही इसकी महत्ता बतायी गयी है-
इष्ट्युपसंख्यानवती शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्था ।
व्युत्पन्नरूपसिद्धिवृत्तिरियं काशिका नाम ॥
वस्तुतः पाणिनीय सूत्रों को समझानेवाली ऐसी कोई वृत्ति नहीं है।
काशिका की दो महत्त्वपूर्ण व्याख्याएँ मिलती हैं- बौद्ध जिनेन्द्रबुद्धि-रचित ‘काशिकाविवरणपञ्जिका’ (अन्य नाम-न्यास) तथा हरदत्त-रचित ‘पदमञ्जरी’। न्यास-टीका का समय ७०० ई. तथा पदमञ्जरी का समय एकादश शतक या इसके कुछ पूर्व हो सकता है।
अष्टाध्यायी की एक वृत्ति ‘भागवृत्ति’ किसी विमलमति नामक विद्वान् की कृति थी जो अब उद्धरण-मात्र में उपलब्ध है। पं. युधिष्ठिर मीमांसक ने ‘भागवृत्ति-संकलन’ के नाम से विभिन्न ग्रन्थों में प्राप्त इसकी पंक्तियों का संग्रह प्रकाशित किया है (१९६४ ई., अजमेर)। इसमें वैदिक तथा लौकिक सूत्रों को पृथक् किया गया है। इसका काल नवम शतक ई. है। बंगाल के निवासी बौद्ध विद्वान् पुरुषोत्तमदेव ने अष्टाध्यायी के केवल लौकिक सूत्रों की वृत्ति ‘भाषावृत्ति’ के नाम से लिखी थी। इन्होंने महाभाष्य की भी व्याख्या लिखी थी (लघुवृत्ति)। अमरकोश के टीकाकार सर्वानन्द (११६० ई.) ने इन ग्रन्थों का बहुधा निर्देश किया है। अतः पुरुषोत्तमदेव का समय ११२० ई. के आसपास सिद्ध होता है। प्रसिद्ध विद्वान् कैयट का भी इन्होंने उल्लेख किया है। पुरुषोत्तम के कुछ परवर्ती बौद्ध विद्वान् शरणदेव (लक्ष्मणसेन के सभापण्डित) ने कुछ अव्याख्येय तथाकथित अपाणिनीय शब्दप्रयोगों की सिद्धि के लिए तदनुकूल ५०० सूत्रों की व्याख्या ‘दुर्घटवृत्ति’ में की। लेखक ने इसकी रचना ११७२ ई. में की थी। जयदेव ने इनके विषय में यथार्थ टिप्पणी की थी- शरण: श्लाघ्यो दुरूहद्रुतेः (अर्थात् शरणदेव व्याकरण के दुरूह प्रयोगों को द्रवित करने या सुगम बनाने में प्रशंसनीय हैं)। गणपति शास्त्री ने त्रिवेन्द्रम् संस्कृत सीरिज में इसका प्रकाशन १९०९ ई. में किया था। भट्टोजिदीक्षित ने भी अष्टाध्यायी की व्याख्या’ शब्दकौस्तुभ’ के रूप में की। यह चतुर्थ अध्याय तक है किन्तु तृतीय अध्याय का उत्तरार्ध (पाद ३-४) नहीं मिले हैं।
महाभाष्य की व्याख्याओं में प्रथम तो भर्तृहरि-कृत’ दीपिका’ है किन्तु यह कुछ ही आह्निकों तक है। महाभाष्य के दो बार लुप्त हो जाने का उल्लेख मिलता है। पहली बार उसका उद्धार चन्द्राचार्य ने किया था (वाक्यपदीय २/४८१ तथा राजतरङ्गिणी १/१७६) । दूसरी बार कश्मीर के राजा जयापीड ने (अष्टम शताब्दी ई.) इसका उद्धार क्षीर उपाध्याय से कराया था (राजत. ४/४८८-९)। कश्मीर के ही निवासी कैयट ने सम्पूर्ण महाभाष्य पर ‘प्रदीप’ व्याख्या लिखकर सदा के लिए लोप और उद्धार की श्रृंखला समाप्त कर दी। पदमञ्जरी के लेखक हरदत्त के ये पूर्ववर्ती थे क्योंकि हरदत्त ने कैयट के मतों का अनेकत्र खण्डन किया है। अत: कैयट का समय १००० ई. से १०५० ई. तक सर्वमान्य है। प्रदीप-टीका के अभाव में महाभाष्य की ग्रन्थियाँ दुर्बोध ही रह जातीं। इसमें कश्मीरी अनुशीलन की परम्परा पुञ्जीभूत हो गयी है। अन्नम्भट्ट (१७ वीं शताब्दी ई.) ने प्रदीप की व्याख्या ‘उद्योतन’ के नाम से लिखी किन्तु सर्वतन्त्रस्वतन्त्र विद्वान् नागेशभट्ट ने (१७०० ई.) इसपर जो ‘उद्योत’ व्याख्या की रचना की वह बहुत प्रसिद्ध हुई। नागेश के शिष्य वैद्यनाथ पायगुण्डे ने इसपर भी टीका लिखी जो नवाह्निक तक मिलती है।
(६) प्रक्रियाग्रन्थ (Sanskrit Vyakaran ka Itihas)
Sanskrit Vyakaran ka Itihas पाणिनीय व्याकरण-परम्परा में त्रिमुनि-काल (६०० ई. पू. से १०० ई. पू.) तथा त्रिमुनि- व्याख्याकाल (१०० ई. पू.-१००० ई.) के बाद प्रक्रियाकाल (१००० ई. के बाद) का आगमन हुआ। अन्य शास्त्रों के समान व्याकरण में भी प्रकरण-ग्रन्थों की आवश्यकता का अनुभव हुआ जिससे अल्पकाल में कुछ कार्यसाधक (working) ज्ञान प्राप्त कर अन्य शास्त्रों के अध्ययनार्थ प्रस्तुत हो सकें। पाणिनीय तन्त्र से बाहर व्याकरण-प्रस्थानों में कालाप-तन्त्र पहले ही प्रकरण के रूप में ही विकसित हो चुका था (१०० ई.)। इन प्रस्थानों में व्याकरण को साध्य न रखकर साधन बनाने पर बल था। संस्कृत भाषा जन-सामान्य में प्रचलित नहीं थी, इसलिए अष्टाध्यायी-जैसे शास्त्रग्रन्थ भाषा-वर्णन के निमित्त अनुपयोगी हो रहे थे, शास्त्रैकदेश का उपदेश देनेवाले प्रकरण-ग्रन्थ’ ही युग पर छा रहे थे। तदनुसार अष्टाध्यायी के सूत्रों का क्रम तोड़कर संज्ञा, सन्धि, समास, कारक, सुबन्त, तिङन्त, तद्धित, कृदन्त, स्त्रीप्रत्यय आदि प्रकरणों में सूत्रों को सजाकर शब्दरूपों की सिद्धि पर ध्यान देना आवश्यक लगा। इससे नव्य पाणिनीय या प्रक्रिया-परम्परा का प्रवर्तन हुआ। इस परम्परा में कई ग्रन्थ विकसित हुए।
इस परम्परा का प्रथम उपलब्ध ग्रन्थ ‘रूपावतार’ है जिसे सिंहली बौद्ध विद्वान् धर्मकीर्ति ने प्रायः ११०० ई. में लिखा था।’ इसमें प्रकरणों के नाम ‘अवतार’ से युक्त हैं- संज्ञावतार, संहितावतार, विभक्त्यवतार इत्यादि। सिद्धान्तकौमुदी के समान उत्तरभाग धातुओं और तद्विहित प्रत्ययों का है। स्वर-वैदिक अंश नहीं है। उणादि पर भी पृथक् परिच्छेद नहीं है। सूत्रों की संक्षिप्त वृत्ति उदाहरण-सहित दी गयी है। १४ वीं शताब्दी के विद्वान् संन्यासी विमलसरस्वती (सूरि) ने इसी ढंग की पुस्तक ‘रूपमाला’ लिखी।’ ‘रूपावतार’ में जहाँ २६६४ सूत्रों की व्याख्या थी वहाँ इसमें केवल २०४६ सूत्र ही रखे गये। इस प्रकार लाघव का प्रयास किया गया। इसमें प्रकरणों के नाम ‘माला’ से युक्त हैं- संज्ञामाला, सन्धिमाला इत्यादि। इन दोनों ग्रन्थों का अधिक प्रचार नहीं हो सका।
आन्ध्रप्रदेश के निवासी ऋग्वेदी ब्राह्मण रामचन्द्र (१४ वीं शताब्दी ई.) ने’ प्रक्रियाकौमुदी ” नामक ग्रन्थ लिखा जिसमें २४७० सूत्रों की वृत्ति और उदाहरण हैं। पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध के रूप में यह भी विभक्त है। क्रम सिद्धान्तकौमुदी के समान है। रामचन्द्र ने वैष्णव-परक उदाहरण दिये हैं। ग्रन्थ के संक्षिप्त होने का कारण ग्रन्थकार ने अन्त में दिया है-
आनन्त्यात्सर्वशब्दा हि न शक्यन्तेऽनुशासितुम् ।
बालव्युत्पत्तयेऽस्माभिः संक्षिप्योक्ता यथामति ॥
प्रक्रियाकौमुदी के लेखक के पौत्र विट्ठल ने इसपर ‘प्रसाद’ नामक टीका लिखी। पुनः भट्टोजिदीक्षित के गुरु शेषकृष्ण ने इसपर ‘प्रकाश’ नामक व्याख्याग्रन्थ लिखा। बीरबल के पुत्र कल्याण को संस्कृत व्याकरण सिखाने के लिए यह व्याख्या लिखी गयी थी। लेखक ने बीरबल का वृंशवृक्ष भी इसके आरम्भ में दिया है। प्रक्रियाकौमुदी में पाणिनीयेतर वैयाकरणों का भी समर्थन है।
पाणिनीय व्याकरण-तन्त्र में भट्टोजिदीक्षित का आविर्भाव बहुत महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने व्याकरण के अतिरिक्त भी कई शास्त्रों में ग्रन्थलेखन द्वारा उनकी श्रीवृद्धि की। आन्ध्रप्रदेश के तैलंग- ब्राह्मणकुल में उत्पन्न भट्टोजिदीक्षित का वंश अनेक वैयाकरणों से समृद्ध था। लक्ष्मीधर भट्ट (पिता), रंगोजीभट्ट (भ्राता), भानुजीदीक्षित (पुत्र), कौण्डभट्ट (भतीजा) तथा हरिदीक्षित (पौत्र) महान् वैयाकरण थे। भट्टोजि ने शेषकृष्ण से व्याकरण और धर्मशास्त्र, नृसिंहाश्रम से वेदान्त तथा अप्पयदीक्षित से मीमांसा का अध्ययन किया था। काशी में रहकर ही इन्होंने अनेक शास्त्रों में मौलिक तथा टीकाग्रन्थ लिखे, किन्तु इन्हें विशेष ख्याति व्याकरण में (मुख्यतः ‘सिद्धान्तकौमुदी’ के कारण) ही मिली। ये खण्डन-रसिक विद्वान् थे; इसलिए प्रखर शब्दों में इन्होंने काशिका, न्यास, पदमञ्जरी तथा अपने गुरु की ‘प्रकाश’-टीका तक का खण्डन किया है। वे कैयट से लेकर सभी वैयाकरणों के ग्रन्थों को शिथिल कहते हैं- तस्मात्कैयटप्रभृत्यर्वाचीनपर्यन्तं सर्वेषां ग्रन्था इह शिथिला एवेति स्थितम् (प्रौढमनोरमा, उत्तरभाग, पृ. ७४२)।
भट्टोजिदीक्षित का काल प्रायः निश्चित है। इनके गुरु नृसिंहाश्रम ने १५४७ ई. में ‘वेदान्ततत्त्वविवेक’ नामक ग्रन्थ लिखा था जिसकी व्याख्या उन्होंने ही दूसरे वर्ष ‘दीपन’ नाम से लिखी। भट्टोजि ने ‘वाक्यमाला’ नामक टीका इस दीपन के ऊपर लिखी। भट्टोजि के एक शिष्य नीलकण्ठ शुक्ल ने ‘शब्दशोभा’ नामक व्याकरण-ग्रन्थ १६३७ ई. में लिखा था। म.म. हरप्रसाद शास्त्री ने उल्लेख किया है कि ‘शब्दकौस्तुभ’ (भट्टोजि की कृति) क़ा एक हस्तलेख १६३३ ई. का मिला है। इस आधार पर पं. बलदेव उपाध्याय ने भट्टोजिदीक्षित का काल १५६० ई. तथा १६१० ई. के बीच माना है।
भट्टोजिदीक्षित ने धर्मशास्त्र (आशौच प्रकरण, तिथिनिर्णय और त्रिस्थलीसेतु), वेदान्त (तत्त्वकौस्तुभ, वाक्यमाला, अद्वैतकौस्तुभ) तथा कुछ अन्य शास्त्रों में भी (तन्त्राधिकार, वेदभाष्यसार, तत्त्वसिद्धान्तदीपिका तथा तैत्तिरीयभाष्य) ग्रन्थों की रचना की। व्याकरण में इनके चार ग्रन्थ हैं – वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, प्रौढमनोरमा, शब्दकौस्तुभ तथा वैयाकरणसिद्धान्तकारिका (भूषणकारिका)।
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इनका प्रसिद्धतम ग्रन्थ है। इसमें पाणिनि के सभी सूत्र प्रक्रियाक्रम से विवेचित हैं, सबकी संक्षिप्तवृत्ति देते हुए परिनिष्ठित रूपों की सिद्धि में उनका विनियोग दिखाया गया है। इसके पूर्वार्ध में संज्ञा, परिभाषा, सन्धि, सुबन्त, अव्यय, स्त्रीप्रत्यय, कारक, समास, तद्धित और द्विरुक्तप्रकरण हैं। उत्तरार्ध में गणों के आधार पर तिङन्त-प्रकरण, प्रत्ययान्त धातुरूप (सनादि, यङ्, नामधातु आदि), लकारार्थ, कृत्य, पूर्वकृदन्त, उणादि, उत्तरकृदन्त, वैदिकप्रकरण तथा स्वरप्रकरण है। इसके अन्त में लिङ्गानुशासन का भी विवेचन है। प्रक्रिया-ग्रन्थों में सिद्धान्तकौमुदी उत्कृष्ट तथा लोकप्रिय है। इसके द्वारा अष्टाध्यायी की शास्त्र- परम्परा उखाड़ दी गयी। इसकी व्याख्याओं में स्वयं भट्टोजिरचित प्रौढमनोरमा, नागेश-कृत शब्देन्दुशेखर (लघु तथा बृहत् संस्करण), वासुदेव दीक्षित कृत बालमनोरमा तथा ज्ञानेन्द्र सरस्वती कृत तत्त्वबोधिनी प्रमुख हैं।
प्रौढमनोरमा उपर्युक्त सिद्धान्तकौमुदी की लेखक-कृत व्याख्या है किन्तु स्वतन्त्र ग्रन्थ का रूप लेती है। इसमें लेखक ने ‘यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्’ का स्पष्ट समर्थन किया है। दुर्घट प्रयोगों को भी समझाने का प्रयास लेखक ने किया है। शेषकृष्ण की प्रकाश-व्याख्या के खण्डनों को इसमें देखकर उनके शिष्योपशिष्य पण्डितराज जगन्नाथ ने ‘प्रौढमनोरमाखण्डन’ नामक ग्रन्थ लिखा जिसमें इसकी आलोचना है। शब्दकौस्तुभ भट्टोजिदीक्षित का शास्त्रानुकूल ग्रन्थ है जो अष्टाध्यायी के सूत्रों की उसी क्रम से व्याख्या है, उसपर विकसित सभी टीकाओं से यह अनुप्राणित है। दुर्भाग्य है कि ग्रन्थ केवल साढ़े तीन अध्यायों के रूप में (तृतीयाध्याय के द्वितीय पाद तक एवं पूरा चतुर्थ अध्याय) मिला है। शेष भाग नष्ट हो गये या लिखे ही नहीं गये। दीक्षित को इस ग्रन्थ से विशेष अनुराग था जैसाकि सिद्धान्तकौमुदी के अन्त में उनका कथन है-
इत्थं लौकिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दर्शितम् ।
विस्तरस्तु यथाशास्त्रं दर्शितः शब्दकौस्तुभे ॥
भट्टोजि की एक लघुकृति ‘वैयाकरणसिद्धान्तकारिका’ है जिसमें केवल ७४ अनुष्टुप्- पद्य हैं; धात्वर्थ, लकारार्थ, सुबर्थ, नामार्थ, समासशक्ति आदि विषयों का विवेचन करते हुए अन्त में स्फोट का प्रकरण है। इस पर रंगोजी के पुत्र (अर्थात् भट्टोजि के भतीजे) कौण्डभट्ट ने ‘वैयाकरणभूषण’ नामक व्याख्या लिखी जो स्वतन्त्र रूप में व्याकरण-दर्शन का महार्ह ग्रन्थ है। इसका संक्षिप्त रूप ‘वैयाकरणभूषणसार’ है जिस पर अनेक टीकाएँ प्रचलित हैं- दर्पण (ले.हरिवल्लभ), भैरवी (भैरवमिश्र), काशिका (हरिराम काले) इत्यादि। इसकी हिन्दी-व्याख्याएँ भी प्रकाशित हैं।
दीक्षित-परिवार के ही हरिदीक्षित ने प्रौढमनोरमा की व्याख्या ‘शब्दरत्न’ के नाम से लिखी जिसके बृहत् और लघु दो संस्करण हुए। इनके शिष्य नागेशभट्ट थे (१६६०-१७२५ ई. के बीच) जिन्होंने अनेक बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे। सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्या शब्देन्दुशेखर (बृहत् और लघु), परिभाषेन्दुशेखर (परिभाषा-रूप वाक्यों की व्याख्या)’, महाभाष्य के प्रदीप को टीका (उद्योत), स्फोटवाद, वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा (मूल, लघु तथा परमलघु- ३ संस्करण) नागेश के मुख्य ग्रन्थ हैं। ये सभी प्रकाशित हैं।’ मञ्जूषा’ व्याकरण-दर्शन का शिखर-ग्रन्थ है। इसके लघुसंस्करण पर कला (वैद्यनाथ पायगुण्ड-कृत) और कुंजिका (कृष्णमित्र-कृत) दो टीकाएँ प्रकाशित हैं (काशी, १९२५ ई.) । ‘परमलघुमञ्जूषा’ लोकप्रिय ग्रन्थ है, इसकी कई टीकाएँ और अनुवाद भी प्रकाशित हैं।
भट्टोजिदीक्षित के प्रख्यात शिष्य वरदराज ने सिद्धान्तकौमुदी के तीन संक्षिप्त संस्करण निर्मित किये जो प्रक्रिया-पद्धति के प्रवेशद्वार माने जाते हैं- सारसिद्धान्तकौमुदी, लघुसिद्धान्तकौमुदी तथा मध्यसिद्धान्तकौमुदी। ये ग्रन्थ क्रमशः बड़े होते गये हैं। इनमें लघुकौमुदी पाणिनीय व्याकरण की आरम्भिक शिक्षा के लिए बहुत प्रचलित है। वरदराज की एक रचना ‘गीर्वाणपदमञ्जरी’ है जिसमें काशी की सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत करने वाले उदारहण दिये गये हैं। इसका प्रकाशन बड़ौदा विश्वविद्यालय से हुआ है। लघुकौमुदी का एक हस्तलेख १६२४ ई. का है (अमेरिका में सुरक्षित)। अतः वरदराज का समय १६००-१६३० ई. तक माना जा सकता है।
केरल के नारायण भट्ट भी भट्टोजिदीक्षित के समकालिक थे। इनका ‘प्रक्रियासर्वस्व’ विशाल ग्रन्थ है जिसमें बीस खण्डों में सम्पूर्ण शब्द-प्रक्रिया को बताया गया है। भोज के व्याकरण- ‘ग्रन्थ ‘सरस्वतीकण्ठाभरण’ पर नारायणभट्ट को पूर्ण आस्था है। यद्यपि महाभाष्य और काशिका इसके मुख्य आधार हैं तथापि लेखक ने अन्य व्याकरण-सम्प्रदायों के मतों का भी ग्रहण किया है। यह ग्रन्थ १९५४ ई. में अनन्तशयनग्रन्थावलि में केवल सुबन्तखण्ड के रूप में प्रकाशित हुआ, इसके तद्धित तथा उणादिखण्ड मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित हैं। शेष भाग अप्रकाशित हैं। इस प्रकार प्रक्रिया-ग्रन्थों की लम्बी परम्परा है।
(७) अन्य ग्रन्थ (Sanskrit Vyakaran ka Itihas)
Sanskrit Vyakaran ka Itihas पाणिनीय व्याकरण-तन्त्र में अन्य अनेक विषयों पर भी ग्रन्थ मिलते हैं जो उक्त साहित्य के पूरक हैं। पाणिनीय धातुपाठ पर अनेक आचार्यों ने टीकाएँ या समीक्षाएँ लिखी जिनमें क्षीरस्वामी (११वीं शताब्दी ई. के उत्तरार्ध में, कश्मीर निवासी) की ‘क्षीरतरङ्गिणी’, मैत्रेयरक्षित (११२५ ई. के निकट, बौद्ध विद्वान्) का ‘धातुप्रदीप’, माधवाचार्य (१४ वीं शताब्दी, सायण की रचना) कृत ‘माधवीयधातुवृत्ति’ प्रमुख हैं।’ इसी प्रकार गणपाठ के शब्दों की व्याख्या करनेवाला एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है – गणरत्नमहोदधि। इसके रचयिता का नाम वर्धमान है। इस ग्रन्थ का रचनाकाल ११४० ई. है। इसमें पाणिनीय गणपाठ के अतिरिक्त शब्दों की भी व्याख्या है। वर्धमान सिद्धराज जयसिंह के राज्यकाल में थे अतः उनके आश्रित हेमचन्द्र से वे पूर्ण परिचित थे। अपने पद्यात्मक ग्रन्थ की व्याख्या भी लेखक ने ही की है। लिङ्गानुशासन पर पाणिनि के सूत्रों के अतिरिक्त वररुचि, हर्षवर्धन, वामन, दुर्गसिंह (कातन्त्र व्याकरण से सम्बद्ध) तथा हेमचन्द्र के ‘लिङ्गानुशासन’ नामक ग्रन्थ हैं।
‘परिभाषा’ व्याकरण का एक महत्त्वपूर्ण विषय है- नियम न होने की स्थिति में नियम निर्धारित करना परिभाषा का कार्य है (अनियमे नियमकारिणी परिभाषा)। यह एक प्रकार से’ भाषा की परिभाषा’ है। कुछ परिभाषाएँ पाणिनि के सूत्रों के रूप में ही हैं। कुछ लोकन्यायसिद्ध हैं, कुछ सूत्रों से ज्ञापित होती हैं तो कुछ परिभाषाएँ वार्तिकों और भाष्य में हैं। सूत्रेतर परिभाषाओं को अनेक आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में विवेचित किया है। यद्यपि पूना से प्रकाशित ‘परिभाषासंग्रह’ में अनेक ग्रन्थों का संकलन है। किन्तु तीन ग्रन्थ मुख्य हैं- पुरुषोत्तम (११५०-१२०० ई.) कृत ‘लघुवृत्ति’, सीरदेव (१३०० ई.) कृत ‘परिभाषावृत्ति’ तथा नागेशभट्ट (१६६०-१७२५ ई.) कृत ‘परिभाषेन्दुशेखर’ (१३३ परिभाषाओं का विवेचन)। अन्तिम ग्रन्थ वैयाकरणों के बीच बहुत प्रचलित है; इसकी टीकाएँ गदा (वैद्यनाथ), भैरवी (भैरवमिश्र), त्रिपथगा (राघवेन्द्राचार्य), भूति (रामकृष्णशास्त्री), विजया (जयदेवमिश्र) आदि हैं। इसकी हिन्दी व्याख्या हर्षनाथ मिश्र ने लिखी है।
इस प्रकार पाणिनीय व्याकरण-तन्त्र अपनी व्यापकता और सर्वाङ्गपूर्ण साहित्य के कारण बहुत महत्त्व रखता है।
इसे भी पढ़े 👉🏻 संस्कृत साहित्य का इतिहास
(८) अन्य व्याकरण-प्रस्थान (Sanskrit Vyakaran ka Itihas)
Sanskrit Vyakaran ka Itihas इस समय पाणिनि से भिन्न दस व्याकरण-प्रस्थान (Schools of grammar) न्यूनाधिक रूप से उपलब्ध तथा प्रचलित हैं- कातन्त्र, चान्द्र, जैनेन्द्र, जैन शाकटायन, भोज, हैम, जौमर, सारस्वत, मुग्धबोध तथा सौपद्म। कातन्त्र या कालाप व्याकरण प्रक्रिया-क्रम से १४१२ सूत्रों के मूल ग्रन्थ पर आश्रित है। यह चार अध्यायों में विभक्त है, प्रथम तीन अध्याय शर्ववर्मा (प्रथम श. ई.) तथा अन्तिम अध्याय किसी कात्यायन के द्वारा रचित है। सूत्र पाणिनीय सूत्रों के आधार पर रचे गये हैं। बिहार, बंगाल तथा गुजरात में इसका प्रचार रहा है। इस पर दुर्गसिंह (६०० ई.) की वृत्ति है जिसपर उग्रभूति, त्रिलोचनदास, जगद्धर भट्ट (कश्मीरी, १३०० ई.) आदि ने टीकाएँ लिखीं। इस प्रस्थान में भी अनेक प्रकरण-ग्रन्थ लिखे गये। जगदीश तर्कालंकार ने ‘शब्दशक्तिप्रकाशिका’ इसी प्रस्थान के अन्तर्गत लिखी है। चान्द्रव्याकरण चन्द्रगोमी ने प्राय: ४०० ई. में लिखा था, ये बौद्ध विद्वान् थे। इसका प्रचार बौद्ध क्षेत्रों में (कश्मीर, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका) ही है। इसमें ‘ त्रिमुनि व्याकरण’ का पूरा उपयोग है किन्तु संज्ञा-शब्दों का प्रयोग नहीं है। सम्प्रति इसमें ६ अध्याय और ३१०० सूत्र मिलते हैं। इस प्रस्थान का ‘काशिका’ में अनेकत्र खण्डन है। इसका एक संक्षिप्त रूप १२०० ई. में भिक्षु काश्यप ने ‘बालावबोधन’ लिखा जो श्रीलंका में संस्कृत-शिक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। जैनेन्द्रव्याकरण के प्रवर्तक पूज्यपाद देवनन्दि (४५० ई.) हैं जिनका ‘ जैनेन्द्रशब्दानुशासन’ अष्टाध्यायी के आदर्श पर लिखा गया ग्रन्थ है। इसके औदीच्य संस्करण में ३००० और दाक्षिणात्य संस्करण में ३७०० सूत्र हैं (दक्षिणात्य सं. में कुछ वार्तिक भी सूत्र-रूप में हैं)। दोनों संस्करणों पर अनेक टीकाएँ मिलती हैं।
जैनशाकटायन प्रस्थान का आचार्य पाल्यकीर्ति (८१४-६७ ई.) ने प्रवर्तन किया था। शाकटायन शब्दानुशासन में ४-४ पादों वाले ४ अध्याय हैं जिन्हें ‘सिद्धि’ नाम से अधिकरणों में विभक्त किया गया है। प्रभाचन्द्र (१००० ई.) ने जैनेन्द्र और शाकटायन दोनों पर वृत्तियाँ लिखी हैं। यक्षवर्मा ने शाकटायनव्याकरण की ‘चिन्तामणि’ टीका लिखी जिसमें कहा गया है कि इसके अभ्यास से बच्चे और स्त्रियाँ भी एक वर्ष में ही संस्कृत समझने लगेंगी।’ इस प्रस्थान में अनेक प्रकरण-ग्रन्थ भी हैं। महाराज भोज ने अपने ‘सरस्वतीकण्ठाभरण’ नामक व्याकरण-ग्रन्थ में आठ अध्यायों में ६४११ सूत्र दिये हैं। सात अध्याय संस्कृत व्याकरण के और अष्टम अध्याय वैदिक व्याकरण का है। व्याकरण के सहायक गणपाठ, परिभाषा, उणादि, लिंगानुशासन- ये सब इसी में समाविष्ट हैं, पृथक् नहीं हैं। आकार-वैपुल्य से यह लोकप्रिय नहीं हो सका यद्यपि तीन टीकाएँ भी लिखी गयीं। भोज का राज्यकाल १०२८ ई. से १०६३ ई. तक था। प्रसिद्ध जैन विद्वान् हेमचन्द्रसूरि ने (१०८८-११७२ ई.) ‘सिद्धहैमशब्दानुशासन’ ग्रन्थ के द्वारा हैम-प्रस्थान का प्रवर्तन किया। गुर्जरनरेश सिद्धराज के आदेश से यह ग्रन्थ लिखा गया। ४-४ पादों के आठ अध्याय इसमें भी भोज- व्याकरण के समान हैं किन्तु आठवें अध्याय में अनेक प्रकार की प्राकृत भाषाओं का व्याकरण है। सात अध्यायों में ३५६६ सूत्र हैं, प्राकृत भाग में १११९ सूत्र हैं। इस पर भी अनेक टीकाएँ हैं।\
१३ वीं शताब्दी ई. में क्रमदीश्वर ने ‘संक्षिप्तसार’ नामक ग्रन्थ के द्वारा एक नये प्रस्थान को जन्म दिया जिसकी स्वोपज्ञ वृत्ति का परिष्कार जुमरनन्दि (१४ वीं शताब्दी) के द्वारा होने से इसे जौमर-प्रस्थान कहते हैं। प्रक्रिया-क्रम से लिखित इस व्याकरण का प्रचार केवल बंगाल में है। सारस्वत-प्रस्थान वस्तुतः नरेन्द्र नामक विद्वान् के द्वारा रचित ७०० सूत्रों से प्रवृत्त हुआ (जो आज अप्राप्य है) किन्तु इसके आधार पर १३ वीं शताब्दी ई. में अनुभूतिस्वरूपाचार्य ने ‘सारस्वत- प्रक्रिया’ लिखी जिसपर अनेक टीकाएँ हैं। भट्टोजिदीक्षित के शिष्य रघुनाथ ने इसपर ‘लघुभाष्य’ लिखा। इस प्रस्थान का एक ग्रन्थ ‘सिद्धान्तचन्द्रिका’ भी है। कई प्रदेशों में प्रक्रिया और चन्द्रिका का पठन-पाठन होता रहा है। ‘मुग्धबोध’ नामक अत्यन्त संक्षिप्त व्याकरण-ग्रन्थ के द्वारा बोपदेव (१३०० ई.) ने एक नूतन प्रस्थान का प्रवर्तन किया। नवद्वीप (पश्चिम बंगाल) तक ही इसका अध्ययन सीमित है। १५ वीं शताब्दी ई. में पद्मनाभदत्त ने ‘सुपद्म’ नामक व्याकरण लिखकर सौपद्म- प्रस्थान संस्कृत व्याकरण को दिया। इसका प्रचार मिथिला में था, अब समाप्त हो गया है।
इस प्रकार संस्कृत व्याकरण में अनेक प्रस्थान देश-विशेष और काल-विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विकसित हुए। आधुनिक युग में प्रक्रियानुसारी व्याकरण अंग्रेजी- हिन्दी आदि भाषाओं में लिखे गये हैं। फिर भी प्राचीन ग्रन्थों का अनुशीलन उच्चतर कक्षाओं में होता है।
दोस्तों ये था संस्कृत व्याकरण का इतिहास उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद 🙏🏻